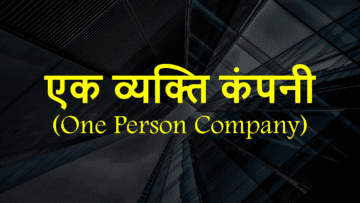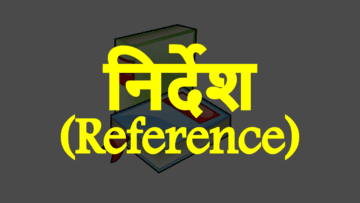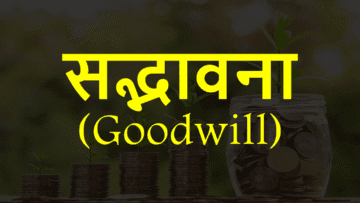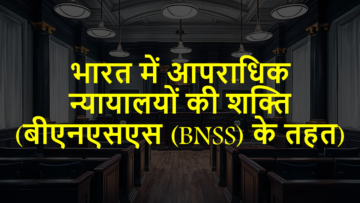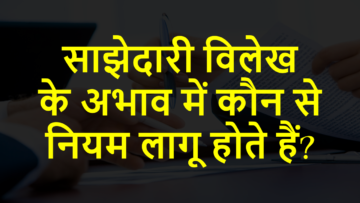कंपनी किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह व्यवसाय का एक रूप है जो कानून द्वारा शासित होता है। भारत में, कंपनी से संबंधित मामले कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा शासित होते हैं, और इसमें कंपनियों के संबंध में विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं।
कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को विभिन्न लाभ मिलते हैं जैसे कि एक अलग कानूनी पहचान, सामान्य मुहर, सीमित देयता, मुकदमा करने की क्षमता, शाश्वत उत्तराधिकार, साथ ही उनसे संबंधित दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता जैसे कि रिपोर्ट का प्रकाशन (यदि आवश्यक हो), पारदर्शिता, औपचारिकताएं, आदि।
कंपनी की अवधारणा के बेहतर उपयोग के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 में विभिन्न प्रकार की कंपनियों को प्रदान किया है, जिन्हें कंपनियों का वर्गीकरण भी कहा जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही प्रकार की कंपनी चुन सके। एक व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सहयोगी कंपनी, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी, असीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सरकारी कंपनी और निधि कंपनी आदि कंपनी अधिनियम, 2013 में दिए गए कंपनियों के प्रकारों के उदाहरण हैं।
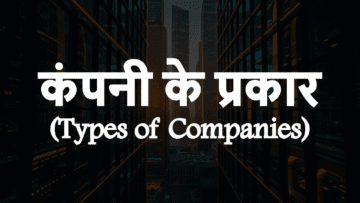
Table of Contents
कंपनियों के प्रकार (Types of Companies)
कंपनियों के प्रकार निम्नलिखित हैं:
| निगमन के आधार पर (Based on Incorporation) | – चार्टर्ड कंपनियां (Chartered Companies) – वैधानिक कंपनियां (Statutory Companies) – पंजीकृत कंपनियां (Registered Companies) |
| सदस्यों के आधार पर (Based on Members) | – एक व्यक्ति कंपनी (One Person Company) – प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company) – पब्लिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company) |
| दायित्व के आधार पर (Based on Liability) | – शेयरों द्वारा सीमित कंपनी (Company Limited By Shares) – गारंटी द्वारा सीमित कंपनी (Company Limited by Guarantee) – असीमित कंपनी (Unlimited Company) |
| आकार के आधार पर (Based on Size) | – सूक्ष्म कंपनियां (Micro Companies) – छोटी कंपनियां (Small Companies) – मध्यम कंपनियां (Medium Companies) – बड़ी कंपनियां (Large Companies) |
| नियंत्रण के आधार पर (Based on Control) | – होल्डिंग कंपनी (Holding Company) – सहायक कंपनी (Subsidiary Company) – सहयोगी कंपनी (Associate Company) |
| सूचीकरण के आधार पर (Based on Listing) | – सूचीबद्ध कंपनी (Listed Company) – असूचीबद्ध कंपनी (Unlisted Company) |
| अन्य कंपनियां (Other Companies) | – सरकारी कंपनी (Government Company) – विदेशी कंपनी (Foreign Company) – निष्क्रिय कंपनी (Dormant Company) – निधि कंपनी (Nidhi Company) – धारा 8 कंपनी (Section 8 Company) |
1. निगमन के आधार पर (Based on Incorporation)
निगमन के आधार पर कंपनी को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है चार्टर्ड कंपनियां, वैधानिक कंपनियां और पंजीकृत कंपनियां:
(I) चार्टर्ड कंपनियां (Chartered Companies)
चार्टर्ड कंपनी एक प्रकार की कंपनी है जो राज्य के शाही चार्टर के आदेश द्वारा बनाई जाती है, और सभी नियम और विनियम शाही चार्टर या विशेष प्रावधानों के मार्गदर्शन में तैयार किए जाते हैं। यह अवधारणा मुख्य रूप से यूरोप में शुरुआती आधुनिक युग में विकसित हुई और दुनिया भर में फैल गई, मुख्य रूप से उन देशों में जहां उनका शासन था। भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थापित पहली चार्टर्ड कंपनी थी, लेकिन अब भारत में ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं है।
(II) वैधानिक कंपनियां (Statutory Companies)
वैधानिक कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो किसी क़ानून के ज़रिए या किसी विशेष अधिनियम को पारित करके बनाई जाती है, और इसका गठन सामान्य कंपनी गठन से काफ़ी अलग होता है क्योंकि इसे बनाने के लिए पहले संसद (केंद्र) या विधानमंडल (राज्य) में एक विशेष अधिनियम पारित करने की ज़रूरत होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय खाद्य निगम (FCI), भारतीय स्टेट बैंक (SBI), जीवन बीमा निगम (LIC), पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (PSIDC), पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL), आदि वैधानिक कंपनी के उदाहरण हैं।
(III) पंजीकृत कंपनियां (Registered Companies)
पंजीकृत कंपनी का मतलब है कंपनी कानून के तहत पंजीकृत कंपनी। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, धारा 8 कंपनी (NGO), आदि। भारत में इस प्रकार की कंपनी बनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में दिए गए सभी प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य है, जैसे AOA, MOA, सदस्यों की संख्या, निदेशकों की संख्या, पंजीकरण प्रक्रिया, आदि। यह दुनिया में सबसे आम प्रकार की कंपनी है, और यह सार्वजनिक, निजी या मिश्रित हो सकती है।
2. सदस्यों के आधार पर (Based on Members)
सदस्यों के आधार पर कंपनी को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: एक व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी:
(I) एक व्यक्ति कंपनी (One Person Company)
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यह एक व्यक्ति वाली कंपनी है या केवल एक व्यक्ति से सम्बंधित है। यह एक प्रकार की कंपनी है जिसे बनाने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और इसमें कंपनी की सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एक अलग कानूनी इकाई, एक सामान्य मुहर, शाश्वत उत्तराधिकार, सीमित देयता, आदि। इसे भारत में पहली बार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था।
ध्यान दें: इस कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या केवल एक है। इसमें नाम के बाद नाम प्रत्यय की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, यदि नाम ABC है, तो ABC One Person Company या ABC OPC।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(62) के अनुसार – ““एक व्यक्ति कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें केवल एक व्यक्ति सदस्य के रूप में हो।”
| सदस्यों की न्यूनतम संख्या | 1 |
| सदस्यों की अधिकतम संख्या | 1 |
| निदेशकों की न्यूनतम संख्या | 1 |
| निदेशकों की अधिकतम संख्या | 1 |
| शेयर की हस्तांतरणीयता | नहीं (No) |
| सार्वजनिक या निजी | निजी (Private) |
| नाम प्रत्यय | One Person Company or OPC |
(II) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company)
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक प्रकार की कंपनी है जिसे एक निजी संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इसे बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और सदस्यों की अधिकतम संख्या सीमा 200 है। इसमें कई विशेषताएं हैं जैसे एक अलग कानूनी इकाई, सामान्य मुहर, सीमित देयता, शाश्वत उत्तराधिकार, मुकदमा करने की क्षमता, आदि, और यह भारत में सबसे आम प्रकार की कंपनी है, और अधिकांश स्टार्टअप व्यवसाय भी इसी व्यवसाय रूप के माध्यम से शुरू होते हैं। इसमें नाम के बाद नाम प्रत्यय की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, यदि नाम ABC है, तो ABC Private Limited या ABC Pvt. Ltd.।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(68) के अनुसार – ““निजी कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है, जिसकी न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी निर्धारित की गई हो, तथा जो अपने लेखों के द्वारा, –
- (i) अपने शेयरों को हस्तांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करती हो;
- (ii) एक व्यक्ति कंपनी के मामले को छोड़कर, अपने सदस्यों की संख्या को दो सौ तक सीमित करती हो:
बशर्ते कि जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी कंपनी में एक या अधिक शेयर संयुक्त रूप से रखते हों, उन्हें इस खंड के प्रयोजनों के लिए एकल सदस्य माना जाएगा:
इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि –
- (A) वे व्यक्ति जो कंपनी के रोजगार में हैं; तथा
- (B) वे व्यक्ति जो पूर्व में कंपनी के रोजगार में थे, उस रोजगार में रहते हुए कंपनी के सदस्य थे तथा रोजगार समाप्त होने के बाद भी सदस्य बने रहे हैं,
सदस्यों की संख्या में शामिल नहीं किए जाएंगे; तथा
- (iii) कंपनी की किसी भी प्रतिभूति के लिए जनता को आमंत्रण देने पर रोक लगाता है।“
| सदस्यों की न्यूनतम संख्या | 2 |
| सदस्यों की अधिकतम संख्या | 200 |
| निदेशकों की न्यूनतम संख्या | 2 |
| निदेशकों की अधिकतम संख्या | 15* |
| शेयर की हस्तांतरणीयता | नहीं (No) |
| सार्वजनिक या निजी | निजी (Private) |
| नाम प्रत्यय | Private Limited or Pvt. Ltd. |
(III) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company)
पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक प्रकार की कंपनी है जिसे पब्लिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इसे बनाने के लिए कम से कम 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और सदस्यों की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। यह विभिन्न साधनों के माध्यम से जनता से धन जुटाता है और इसमें कई विशेषताएं होती हैं जैसे एक अलग कानूनी इकाई, शेयरों का हस्तांतरण, सामान्य मुहर, सीमित देयता, शाश्वत उत्तराधिकार, मुकदमा करने की क्षमता, आदि। इसमें नाम के बाद नाम प्रत्यय की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, यदि नाम ABC है, तो ABC Limited या ABC Ltd.।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(71) के अनुसार – ““सार्वजनिक कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो-
- (a) निजी कंपनी नहीं है;
- (b) जिसकी न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी निर्धारित की जा सकती है:
बशर्ते कि कोई कंपनी जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी है, जो निजी कंपनी नहीं है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी, भले ही ऐसी सहायक कंपनी अपने लेखों में निजी कंपनी बनी रहे।“
| सदस्यों की न्यूनतम संख्या | 7 |
| सदस्यों की अधिकतम संख्या | कोई सीमा नहीं (No Limit) |
| निदेशकों की न्यूनतम संख्या | 3 |
| निदेशकों की अधिकतम संख्या | 15* |
| शेयर की हस्तांतरणीयता | हाँ (Yes) |
| सार्वजनिक या निजी | सार्वजनिक (Public) |
| नाम प्रत्यय | Limited or Ltd. |
3. दायित्व के आधार पर (Based on Liability)
दायित्व के आधार पर कंपनी को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: शेयरों द्वारा सीमित कंपनियां, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां और असीमित कंपनियां:
(I) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी (Company Limited By Shares)
शेयरों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब है कि कंपनी के शेयरधारक शेयरों की देयता की सीमाओं द्वारा संरक्षित होते हैं, और यह सदस्यों की देयता के आधार पर कंपनी के प्रकार के रूप में वर्गीकृत है। सरल शब्दों में कहें तो, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब है कि कंपनी के शेयरधारक केवल अपने शेयरों की सीमा तक नुकसान के लिए उत्तरदायी हैं, और कोई भी शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई शेयरधारक 10 रुपये का निवेश करता है, तो वह केवल 10 रुपये के लिए उत्तरदायी होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो, शेयरधारक को केवल उस राशि तक ही नुकसान हो सकता है, जो उसने निवेश की है, उससे अधिक नहीं।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(22) के अनुसार – ““शेयरों द्वारा सीमित कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों की देयता ज्ञापन द्वारा उनके द्वारा धारित शेयरों पर अदा न की गई राशि, यदि कोई हो, तक सीमित होती है।”
(II) गारंटी द्वारा सीमित कंपनी (Company Limited by Guarantee)
गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का मतलब है कि कंपनी के सदस्य सीमा की गारंटी द्वारा संरक्षित हैं, और इसे सदस्यों की देयता के आधार पर कंपनी के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का मतलब है कि कंपनी के सदस्य केवल अपनी गारंटी की सीमा तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, और कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई सदस्य 20 रुपये की गारंटी लेता है, तो वह केवल 20 रुपये के लिए उत्तरदायी होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो, सदस्य केवल उस राशि तक ही नुकसान उठाता है, जिसकी उसने गारंटी दी है, उससे अधिक नहीं।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(21) के अनुसार – ““गारंटी द्वारा सीमित कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों की देयता ज्ञापन द्वारा उस राशि तक सीमित होती है, जिसे सदस्य कंपनी के समापन की स्थिति में कंपनी की परिसंपत्तियों में योगदान करने के लिए क्रमशः वचनबद्ध कर सकते हैं।”
(III) असीमित कंपनी (Unlimited Company)
असीमित कंपनी को कंपनी के सदस्यों की देयता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इसमें सदस्यों की देयता असीमित होती है, जिसका अर्थ है कि सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। कंपनी के अन्य रूपों में सदस्यों को शेयर या गारंटी द्वारा सुरक्षा दी जाती है, लेकिन कंपनी के इस रूप में ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है, सदस्यों की देयता असीमित है। यह रूप केवल एक निजी कंपनी द्वारा अपनाया जाता है, सार्वजनिक कंपनी द्वारा नहीं।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(92) के अनुसार – ““असीमित कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों की देयता पर कोई सीमा नहीं होती है।”
4. आकार के आधार पर (Based on Size)
आकार के आधार पर कंपनी को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: सूक्ष्म कंपनियां, छोटी कंपनियां और मध्यम कंपनियां:
(I) सूक्ष्म कंपनियां (Micro Companies)
सूक्ष्म कंपनियों से तात्पर्य उन कंपनियों से है जिनका निवेश (संपत्ति) ₹1 करोड़ से कम और वार्षिक कारोबार (राजस्व) ₹5 करोड़ से कम है। जो सूक्ष्म कंपनियों अंतर्गत आते हैं, वे सरकार या शासकीय कानून से कम अनुपालन, सब्सिडी, कर लाभ, आदि जैसे कुछ विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं।
| निवेश (Investment) | – ₹1 करोड़ से कम |
| कारोबार (Turnover) | – ₹5 करोड़ से कम |
(II) छोटी कंपनियां (Small Companies)
छोटी कंपनियों से तात्पर्य उन कंपनियों से है जिनका निवेश (संपत्ति) ₹1 करोड़ से अधिक लेकिन ₹10 करोड़ से कम है, और वार्षिक कारोबार (राजस्व) ₹5 करोड़ से अधिक लेकिन ₹50 करोड़ से कम है। जो छोटी कंपनियों के अंतर्गत आती हैं, उन्हें सरकार या शासकीय कानूनों से कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, जैसे कम अनुपालन, सब्सिडी, कर लाभ आदि।
| निवेश (Investment) | – ₹1 करोड़ से अधिक, लेकिन ₹10 करोड़ से कम |
| कारोबार (Turnover) | – ₹5 करोड़ से अधिक, लेकिन ₹50 करोड़ से कम |
(III) मध्यम कंपनियां (Medium Companies)
मध्यम कंपनियों से तात्पर्य उन कंपनियों से है जिनका निवेश (संपत्ति) 10 करोड़ से अधिक है, लेकिन ₹50 करोड़ से कम है और वार्षिक कारोबार (राजस्व) 50 करोड़ से अधिक है, लेकिन ₹250 करोड़ से कम है। जो मध्यम कंपनियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें सरकार या शासन कानून से कम अनुपालन, सब्सिडी, कर लाभ, आदि जैसे कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं।
| निवेश (Investment) | – 10 करोड़ से अधिक, लेकिन ₹50 करोड़ से कम |
| कारोबार (Turnover) | – 50 करोड़ से अधिक, लेकिन ₹250 करोड़ से कम |
(IV) बड़ी कंपनियां (Large Companies)
बड़ी कंपनियों से तात्पर्य उन कंपनियों से है जिनका निवेश (संपत्ति) ₹50 करोड़ से अधिक है, और वार्षिक कारोबार (राजस्व) ₹250 करोड़ से अधिक है। या दूसरे शब्दों में कहें तो, जब कोई मध्यम आकार की कंपनी निर्धारित सीमा पार कर जाती है, तो उसे बड़ी कंपनियों में शामिल किया जाता है। ध्यान दें कि कंपनियों के आकार को मापने के लिए विभिन्न कारकों का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कर्मचारी, क्षेत्र, सेक्टर आदि।
| निवेश (Investment) | – 50 करोड़ से अधिक |
| कारोबार (Turnover) | – 250 करोड़ से अधिक |
5. नियंत्रण के आधार पर (Based on Control)
नियंत्रण के आधार पर कंपनी को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: होल्डिंग कंपनियां और सहायक कंपनियां:
(I) होल्डिंग कंपनी (Holding Company)
होल्डिंग कंपनी का अर्थ मूल कंपनी है जो अन्य कंपनियों के शेयर रखती है, जिसे सहायक कंपनी के रूप में जाना जाता है। होल्डिंग कंपनी के पास सहायक कंपनी के अधिकांश शेयर (आमतौर पर 51% से अधिक) होते हैं। उदाहरण के लिए Alphabet Inc. एक होल्डिंग कंपनी है जो गूगल (Google), वेमो (Waymo), वेरिली (Verily), गूगल फाइबर (Google Fiber), आदि के अधिकांश शेयर रखती है और ये Alphabet Inc. की सहायक कंपनी हैं।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(46) के अनुसार – “एक या एक से अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में “होल्डिंग कंपनी” का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हों।”
(I1) सहायक कंपनी (Subsidiary Company)
सहायक कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसे दूसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे होल्डिंग या मूल कंपनी के रूप में जाना जाता है। एक सहायक कंपनी अपनी मूल कंपनी के अनुसार काम करती है। सहायक कंपनी में अधिकांश शेयर (आमतौर पर 51% से अधिक) उसकी मूल कंपनी या होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं और सहायक कंपनी अपनी मूल कंपनियों को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है। उदाहरण के लिए गूगल (Google), वेमो (Waymo), वेरिली (Verily), गूगल फाइबर (Google Fiber), आदि Alphabet Inc. की सहायक कंपनी हैं।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसार – “किसी अन्य कंपनी (अर्थात होल्डिंग कंपनी) के संबंध में “सहायक कंपनी” या “सहायक” का अर्थ ऐसी कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी-
- (i) निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है; या
- (ii) अपने दम पर या अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ मिलकर कुल मतदान शक्ति के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण करती है:
बशर्ते कि होल्डिंग कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, निर्धारित संख्या से अधिक सहायक कंपनियों की परतें नहीं होंगी।
स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,-
- (a) कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी मानी जाएगी, भले ही उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट नियंत्रण होल्डिंग कंपनी की किसी अन्य सहायक कंपनी का हो;
- (a) किसी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना किसी अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित मानी जाएगी यदि वह अन्य कंपनी अपने विवेकानुसार किसी शक्ति का प्रयोग करके सभी या अधिकांश निदेशकों को नियुक्त या हटा सकती है;
- (c) “कंपनी” में कोई भी निगमित निकाय शामिल है;
- (d) किसी होल्डिंग कंपनी के संबंध में “लेयर” का अर्थ उसकी सहायक या सहायक कंपनियाँ हैं।“
(III) सहयोगी कंपनी (Associate Company)
सहयोगी कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव हो और उस कंपनी के पास इस कंपनी का 20% से ज़्यादा लेकिन 51% से कम हिस्सा हो। सरल शब्दों में कहें तो, सहयोगी कंपनी का मतलब है सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) के अनुसार – “किसी अन्य कंपनी के संबंध में “सहयोगी कंपनी”का अर्थ ऐसी कंपनी है, जिसमें उस अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन जो ऐसे प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें संयुक्त उद्यम कंपनी भी शामिल है।
स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजन के लिए,—
- (a) अभिव्यक्ति “महत्वपूर्ण प्रभाव” का अर्थ है कुल मतदान शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत (20%) का नियंत्रण, या किसी समझौते के तहत व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण या भागीदारी;
- (b) अभिव्यक्ति “संयुक्त उद्यम” का अर्थ है एक संयुक्त व्यवस्था जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों को व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है।”
6. सूचीकरण के आधार पर (Based on Listing)
सूचीकरण के आधार पर कंपनी को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: सूचीबद्ध कंपनियां और गैर-सूचीबद्ध कंपनियां:
(I) सूचीबद्ध कंपनी (Listed Company)
सूचीबद्ध कंपनियों का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों से है, जिसका मतलब है कि कंपनी के शेयर खुले बाजार में बेचे जाते हैं और कोई भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। सूचीबद्ध कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी है और यह अपने नाम के बाद नाम प्रत्यय का उपयोग करती है जैसे “Limited” या “Ltd.”। शेयर के विनिमय/व्यापार से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन देश के एक्सचेंज बोर्ड द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शेयर/स्टॉक ट्रेडिंग से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(52) के अनुसार- ““सूचीबद्ध कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई भी प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है:
बशर्ते कि ऐसी कंपनियों का वर्ग, जिन्होंने प्रतिभूतियों के ऐसे वर्ग को सूचीबद्ध किया है या सूचीबद्ध करने का इरादा रखते हैं, जैसा कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परामर्श से निर्धारित किया जा सकता है, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा।
(II) असूचीबद्ध कंपनी (Unlisted Company)
असूचीबद्ध कंपनियों का मतलब उन कंपनियों से है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं, यानी कंपनी के शेयर खुले बाजार में सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जाते हैं और कोई भी कंपनी के शेयर आसानी से नहीं खरीद सकता है। इसमें बहुत कम निवेशक पाए जाते हैं और वे इसमें बड़ी संख्या में शेयर खरीदते हैं। ध्यान दें: असूचीबद्ध कंपनी निजी या सार्वजनिक कंपनी हो सकती है। हीरो फिनकॉर्प, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, चेन्नई सुपर किंग्स, आदि असूचीबद्ध कंपनियों के उदाहरण हैं।
7. अन्य कंपनियां (Other Companies)
निम्नलिखित भी कम्पनियों के प्रकार हैं:
(I) सरकारी कंपनी (Government Company)
सरकारी कंपनी एक प्रकार की कंपनी है जिसमें सरकार के पास कंपनी का बहुमत हिस्सा होता है जो संभवतः 51% से अधिक होता है और वह कंपनी के मामलों का प्रबंधन करती है। सरकार में राज्य, केंद्र या दोनों शामिल हो सकते हैं और यदि दोनों का कुल हिस्सा 51% से अधिक है तो उस कंपनी को भी सरकारी कंपनी कहा जाता है। इस प्रकार की कंपनी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण और बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है। भारत में, तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय रेलवे, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), आदि सरकारी कंपनियों के उदाहरण हैं।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार- “सरकारी कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है, जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत (51%)चुकता शेयर पूंजी केन्द्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो और इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल है जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो।”
(II) विदेशी कंपनी (Foreign Company)
विदेशी कंपनी का मतलब है किसी दूसरे देश में निगमित कंपनी। उदाहरण के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूनिलीवर, सैमसंग, नेस्ले, टोयोटा, आदि किसी दूसरे देश में निगमित हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी और संचालन भारत में भी है, इस मामले में ये सभी कंपनियां भारत के लिए विदेशी कंपनी हैं। सरल शब्दों में कहें तो, जहां कंपनी निगमित है, उसे घरेलू कंपनी कहा जाता है और अगर वे किसी दूसरे देश में भी संचालन स्थापित करते हैं तो उस देश के लिए वे विदेशी कंपनी बन जाती हैं। भारत में, नई आर्थिक नीति 1991 के बाद विदेशी कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई क्योंकि उस नीति ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(42) के अनुसार- “विदेशी कंपनी” से तात्पर्य भारत के बाहर निगमित किसी भी कंपनी या निगमित निकाय से है, जो-
- (क) भारत में स्वयं या किसी एजेंट के माध्यम से, भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्यवसाय करती है; और
- (ख) किसी अन्य तरीके से भारत में कोई व्यवसायिक गतिविधि संचालित करती है।”
(III) निष्क्रिय कंपनी (Dormant Company)
निष्क्रिय कंपनी एक निष्क्रिय और मौन (Inactive and Silent) कंपनी होती है जो वर्तमान में कोई व्यवसाय या आय उत्पन्न नहीं कर रही होती है, और यह भी एक प्रकार की कंपनी होती है। यह अन्य प्रकार की कंपनियों से काफी अलग होती है क्योंकि इसकी पंजीकरण प्रक्रिया समान होती है, लेकिन अवधारणा अन्य प्रकार की कंपनियों से अलग होती है। इस प्रकार की कंपनी बनाने का मुख्य उद्देश्य भविष्य की परियोजना के लिए होता है, और यह परियोजना शुरू होने तक मौन और निष्क्रिय (आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) रहती है। एक बार जब परियोजना या सामान्य गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं, तो इसे निष्क्रिय कंपनी नहीं कहा जाता है, और यह एक सामान्य कंपनी बन जाती है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455(1) के अनुसार- “जहां कोई कंपनी किसी भावी परियोजना के लिए या किसी परिसंपत्ति या बौद्धिक संपदा को धारण करने के लिए इस अधिनियम के तहत गठित और पंजीकृत की जाती है और उसका कोई महत्वपूर्ण लेखा-जोखा लेन-देन नहीं होता है, ऐसी कंपनी या निष्क्रिय कंपनी निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकती है।
स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—
- (i) “निष्क्रिय कंपनी” का अर्थ ऐसी कंपनी है जो पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या जिसने कोई महत्वपूर्ण लेखा-जोखा लेन-देन नहीं किया है, या जिसने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है;
- (ii) “महत्वपूर्ण लेखा-जोखा लेन-देन” का अर्थ निम्नलिखित के अलावा कोई अन्य लेन-देन है—
- (a) रजिस्ट्रार को कंपनी द्वारा शुल्क का भुगतान;
- (b) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके द्वारा किए गए भुगतान;
- (c) इस अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शेयरों का आवंटन; और
- (d) अपने कार्यालय के रखरखाव के लिए भुगतान अभिलेख.
(IV) निधि कंपनी (Nidhi Company)
निधि कंपनी भारत में एक प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है जो सामुदायिक कल्याण के लिए काम करती है और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी अवधारणा दूसरी NBFC से अलग होती है क्योंकि इसमें केवल सदस्य ही पैसा जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वे इसे निकालते या उधार लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसका लाभ केवल सदस्य ही उठा सकते हैं।
निधि कंपनी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) द्वारा शासित है और इसके नाम के बाद एक नाम प्रत्यय लगाना अनिवार्य होता है, जैसे “Nidhi Limited” या “Nidhi Ltd.”। माबेन निधि लिमिटेड, समर्थ निधि लिमिटेड, महामुद्रा ग्लोबल निधि लिमिटेड, सिद्धिविनायक निधि लिमिटेड, मिनी मुथूट्टू निधि केरल लिमिटेड, आदि निधि कंपनियों के उदाहरण हैं।
(V) धारा 8 कंपनी (Section 8 Company)
सेक्शन 8 कंपनी एक प्रकार की कंपनी है जिसे आम तौर पर गैर-लाभकारी संगठन कंपनी के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण, कला, वाणिज्य, शिक्षा, दान, पर्यावरण संरक्षण, खेल, विज्ञान, अनुसंधान आदि को बढ़ावा देना है। यह कंपनी अपने लाभ को अपने सदस्यों में वितरित नहीं करती है, बल्कि इसे आगे के कल्याण के लिए पुनर्निवेशित करती है और यह कंपनी कर कानून के तहत कर लाभ का आनंद लेती है। इस कंपनी को “प्राइवेट लिमिटेड”, “लिमिटेड” जैसे किसी भी तरह के नाम प्रत्यय का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। टाटा ट्रस्ट, इंफोसिस फाउंडेशन, प्रेमजी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, आगा खान फाउंडेशन, आदि सेक्शन 8 कंपनियों के उदाहरण हैं।
ध्यान दें: उपरोक्त डेटा परिवर्तन के अधीन है।
यह भी पढ़ें:
- कंपनी (Company) क्या है? अर्थ, विशेषताएं और बहुत कुछ।
- कंपनी के फायदे और नुकसान (Advantages and Disadvantages of the Company)
- एक व्यक्ति कंपनी (One Person Company) क्या है? अर्थ, विशेषताएँ, और बहुत कुछ।
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company) क्या है? अर्थ, विशेषताएं और बहुत कुछ।
- पब्लिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company) क्या है? अर्थ, विशेषताएं और बहुत कुछ।
QNA/FAQ
Q1. किस कंपनी को बड़ी कंपनी कहा जाता है?
Ans: वह कंपनी जिसका निवेश (संपत्ति) ₹50 करोड़ से अधिक है, और वार्षिक कारोबार (राजस्व) ₹250 करोड़ से अधिक है, उसे बड़ी कंपनी कहा जाता है।
Q2. सहयोगी कंपनी बनने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत आवश्यक है?
Ans: सहयोगी कंपनी बनने के लिए न्यूनतम 20% शेयरधारिता आवश्यक है।
Q3. किस कंपनी को निष्क्रिय कंपनी (Inactive Company) कहा जाता है?
Ans: निष्क्रिय कंपनी (Dormant Company) को निष्क्रिय कंपनी (Inactive Company) भी कहा जाता है।
Q4. धारा 8 कंपनी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?
Ans: धारा 8 कंपनी का उपयोग सामाजिक कल्याण, कला, वाणिज्य, शिक्षा, दान, पर्यावरण संरक्षण, खेल, विज्ञान, अनुसंधान आदि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
Q5. कंपनियों का वर्गीकरण लिखिए।
Ans: कंपनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित हैं:
1. निगमन के आधार पर (Based on Incorporation)
– चार्टर्ड कंपनियां (Chartered Companies)
– वैधानिक कंपनियां (Statutory Companies)
– पंजीकृत कंपनियां (Registered Companies)
2. सदस्यों के आधार पर (Based on Members)
– एक व्यक्ति कंपनी (One Person Company)
– प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company)
– पब्लिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company)
3. दायित्व के आधार पर (Based on Liability)
– शेयरों द्वारा सीमित कंपनियां (Companies Limited By Shares)
– गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां (Companies Limited by Guarantee)
– असीमित कंपनी (Unlimited Company)
4. आकार के आधार पर (Based on Size)
– सूक्ष्म कंपनियां (Micro Companies)
– छोटी कंपनियां (Small Companies)
– मध्यम कंपनियां (Medium Companies)
– बड़ी कंपनियां (Large Companies)
5. नियंत्रण के आधार पर (Based on Control)
– होल्डिंग कंपनी (Holding Company)
– सहायक कंपनी (Subsidiary Company)
– सहयोगी कंपनी (Associate Company)
6. सूचीकरण के आधार पर (Based on Listing)
– सूचीबद्ध कंपनी (Listed Company)
– असूचीबद्ध कंपनी (Unlisted Company)
7. अन्य कंपनियां (Other Companies)
– सरकारी कंपनी (Government Company)
– विदेशी कंपनी (Foreign Company)
– निष्क्रिय कंपनी (Dormant Company)
– निष्क्रिय कंपनी (Nidhi Company)
– धारा 8 कंपनी (Section 8 Company)
स्रोत: